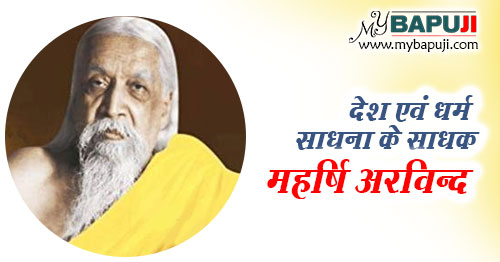Last Updated on August 25, 2019 by admin
स्वामी रामानन्द जी का आलन्दी आगमन :
भक्ति मार्ग के प्रवर्तक प्रसिद्ध धार्मिक सन्त स्वामी रामानन्द काशी से रामेश्वरम् की यात्रा पर निकले थे । मार्ग में एक गाँव पड़ता था आलन्दी । स्वामी रामानन्द ने वहाँ अपना डेरा डाला और कुछ दिनों तक रुक जनसाधारण को ज्ञान-कर्म और भक्ति त्रिवेणी में मज्जित कराते रहे । स्वामी रामानन्द एक मारुति मन्दिर में ठहरे हुए थे, उसी मन्दिर में गाँव की एक युवती स्त्री भी प्रतिदिन दर्शन और पूजन के लिए आया करती थी। संयोग से एक दिन स्वामीजी का उससे सामना हो गया । स्त्री ने रामानन्द जी को प्रणाम किया तो बरबस उनके मुँह से निकल गया- ‘पुत्रवती भव ।’
आशीर्वाद सुनकर युवती पहले तो हँसी फिर एकाएक चुप हो गयी । स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने पूछा- ‘देवी तुम हँसी क्यों हो ? फिर एकाएक चुप क्यों हो गयी ?’
उस युवती ने कहा- ‘मेरी हँसी और फिर चुप्पी का कारण यह है कि आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद बिल्कुल निष्फल जायेगा।’
क्यों बेटी तुम्हारी कोई सन्तान नहीं है क्या- माथे पर सिन्दूर और हाथों में चूड़ियाँ देखकर स्वामी जी ने उसके सधवा होने का अनुमान लगाते हुए कहा ।
तो स्त्री बोली – ‘सन्तान हो भी तो कैसे स्वामी जी । मेरे पति तो वैराग्य धारण कर संन्यासी हो गये हैं । सुना है उन्होंने आप ही से ही दीक्षा ली है।’
‘मुझसे’- स्वामी जी ने चिन्तामग्न होकर पूछा । चिन्ता इसलिए थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तो गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और इस धर्म में अभी ठीक से निर्वाह भी नहीं हुआ था कि उसने पलायन कर लिया और मुझसे ही दीक्षा ग्रहण की । कुछ सोचते हुए स्वामी जी ने पूछा- ‘बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पतिकिस नाम से पुकारे जाते हैं।’
‘मेरा नाम रुक्मिणी है और मेरे पति विट्ठल पन्त कहे जाते हैं- युवती ने कहा- ‘वे एक दिन गंगा स्नान की कह कर गये और फिर कभी नहीं लौटे । लौटे तो उनके समाचार कि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है । तभी से मैं भी आठ पहर में केवल एक बार भोजन करती हूँ। पीपल की प्रदक्षिणा करती हूँ । इस बात को बारह वर्ष हो गये हैं।’
रुक्मिणी अभी २९-३० के लगभग की थी। इसका अर्थ ‘क्या’ कि विठ्ठल पन्त के कारण यह असमय में ही तापस वेश धारण करने के लिए विवश हो गयी थी । स्वामी जी ने कहा- समझ गया । समझ गया । इतने ही वर्ष पूर्व विट्ठल पन्त वे मुझसे संन्यास दीक्षा ली थी और चैतन्याश्रम स्वामी नाम धारण किया था ।
फिर उन्होंने अपनी रामेश्वर यात्रा का विचार निरस्त करते हुए कहा- अब मैं काशी ही जाऊँगा और चैतन्याश्रम को वापस तुम्हारे पास भेजूंगा । जो व्यक्ति सन्तानहीन युवती पत्नी को छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है, शास्त्रों की दृष्टि से वह आश्रम व धर्म की मर्यादा भंग करने वाला पातकी है । उसे दीक्षा देने वाला गुरु भी उस दोष का भागी बनता है।
सन्त ज्ञानेश्वर जी का जन्म :
स्वामी जी के इस निश्चय की सुनकर रुक्मिणी ने भी उनके साथ काशी चलने का विचार व्यक्त किया । अपने माता-पिता की सम्मति लेकर वह उनके साथ काशी गयी । स्वामी जी ने चैतन्याश्रम को बुलाकर सारा हाल पूछा तथा उसे समझा-बुझाकर रुक्मिणी के साथ आलन्दी भेज दिया । चैतन्याश्रम फिर गृहस्थ होकर विट्ठल पन्त हो गये । इन्हीं दम्पत्ति ने सन १२७३ में ज्ञानदेव को जन्म दिया जो सन्त ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे।
संघर्षमय जीवन :
सन्त ज्ञानेश्वर का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हआ जब उनके माता-पिता समाज से बहिष्कृत कर दिये गये थे । स्वामी रामानन्द ने तो विट्ठल पन्त को संन्यास छोड़कर गृहस्थ धर्म का पालन करने की आज्ञा दे दी थी और इसे शास्त्रोचित्त भी बताया था पर महाराष्ट्र के पण्डित इसे सहन नहीं कर पा रहे थे । उस समय किसी संन्यासी का संन्यास छोडकर गहस्थाश्रम में लौट आना एक बहुत अदभुत बात थी और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाता था । समझा जाता था कि इससे संन्यासाश्रम का भी अपमान होता है और गृहस्थाश्रम पर भी कलंक लगता है । इसलिए वहाँ के ब्राह्मण पण्डितों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उन्हें जाति और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाय ।
विट्ठल पन्त जब बहिष्कृत कर दिये गये तो उनकी आलोचना भी खूब हई। पर गुरु द्वारा दी गयी व्यवस्था के कारण लोकापवाद से वे जरा-भी विचलित नहीं हुए । उलटे उनके स्वाध्याय, आत्म चिन्तन और ईश्वर भजन में लगने वाला समय बढ़ता गया । पत्नी भी पति के पद-चिह्नों पर चलने लगी । इस प्रकार एक तरह से सारा परिवार ही भगवद्भक्त बन गया। उस समय विट्ठल पन्त की दशा अत्यन्त शोचनीय चल रही थी । न कहीं काम मिलता और न कोई शिक्षा देता था । फिर भी परम सन्तोषी वृत्ति के विठ्ठल पन्त और उनकी पत्नी रुक्मिणी कई बार पेट की आग को पानी से बुझा लेते।
ज्ञानेश्वर अपने पिता की दूसरी सन्तान थे । उनसे पूर्व निवृत्ति नाथ का जन्म हो चुका था। बाद में एक भाई और बहिन जन्मे । इस प्रकार चार सन्तानों का पेट भरना बड़ा कठिन काम था । इस पर उनके भविष्य की चिन्ता अलग से । यह तो निश्चित था कि बहिष्कृत परिवार की सन्तान होने के कारण चारों को भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। न मिली ही । जब ज्ञानदेव के बड़े भाई निवृत्ति नाथ सात वर्ष के हुए तो विठ्ठल पन्त ने उनका उपनयन कराने का विचार किया । उन्हें पता था कि संस्कार के समय कोई ब्राह्मण नहीं आयेगा । फिर भी उन्होंने अपनी ओर से अनुनय-विनय किया । कोई नहीं आया और निराश होकर विट्ठल पन्त ने पूरे परिवार को लेकर व्यंवकेश्वर चलने का निश्चय किया ।
माता पिता का महाप्रयाण :
वहाँ अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध योगी गहिनीनाथ ने निवृति नाथ को दीक्षा दी । इसके बाद पूरा परिवार अपने गाँव आ गया । वहाँ कुछ दिनों तक रहे । फिर विट्ठल पन्त और रुक्मिणी अपने चार बच्चों को अनाथ छोड़कर प्रयाण कर गये । सब बालक अनाथ और असहाय होकर भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करने लगे । पिता की तरह शास्त्राध्ययन और सत्संग चर्चा में उनकी भी बड़ी रुचि थी । उनकी कुशाग्रबुद्धि को देखकर जहाँ पैठण के ब्राह्मण बड़े प्रभावित होते थे वहीं उनकी दुर्दशा देखकर उन्हें दया भी आती थी ।
कुछ ही वर्षों में ज्ञानदेव ने शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ समाज की स्थिति का भी खुली आँखों से अध्ययन कर लिया । इससे उनकी समझ में यह तथ्य भली-भांति आ गया कि इन दिनों समाज में वर्ण, जाति और आश्रम के अनुसार बड़ा भेद-भाव प्रचलित था।
और इस भेद-भाव के शिकार न केवल वही लोग हुए हैं बल्कि निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग उनसे भी गयी गुजरी स्थिति में हैं । ज्ञानदेव अपने अनुभव भाइयों को भी बताते हैं और सुझाते कि इन भेद-भावों को दूर किया जाना चाहिए । यह सुधार कार्य किस प्रकार हो इसका उचित उपाय यही समझा गया कि समाज में रहते हुए सौम्य और नम उपायों से ही काम लिया जाय।
पैठण के ब्राह्मणों द्वारा सुद्दिपत्र देना :
इधर पैठण के ब्राह्मणों ने भी अच्छी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने निर्णय दिया कि माता-पिता के अपराधों का दण्ड उनकी सन्तानों को देना अन्यायपूर्ण है इसलिए इन चारों भाई-बहिनों की शुद्धि कर समाज में ले लेना चाहिए । तद्नुसार सन् १२८८ में पैठण के ब्राह्मणों ने इन चारों बालकों की शुद्धि करवा कर समाज में सम्मिलित कर लिया ।
ज्ञानेश्वरी-गीता की रचना :
शुद्धि कराकर ज्ञानेश्वर अपने भाई-बहिन सहित वेवा से आ गये और वही रहने लगे । यहीं रहकर ज्ञानेश्वर जी ने भगवद्गीता पर १२९८ में एक सुन्दर भाष्य लिखा । जो ‘ज्ञानेश्वरी गीता’ के नाम से मराठी साहित्य और धर्म ग्रन्थों के भाष्यसाहित्य में आज भी अपना महत्त्व रखता है।
यों ज्ञानेश्वरजी के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारिक घटनायें प्रचलित हैं । पता नहीं वे कितनी सत्य हैं और कितनी असत्य । पर ज्ञानेश्वरी-गीता के नाम से उन्होंने जो ग्रन्थ धार्मिक जनता को दिया वह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है । लगभग ८००० पृष्ठों के इस वृहद् ग्रन्थ में गीता का भावार्थ मराठी के ओवी छन्दों में बड़े सुन्दर ढंग से विश्लेषित किया गया है । अब से लगभग ७०० वर्ष पूर्व लिखी गई इस ज्ञानेश्वर गीता में ४६ भाषाओं के शब्द आये बताये जाते हैं । इसी से पता चलता है कि ज्ञानेश्वर जी ने अल्पायु में ही कितनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
जिस समय ज्ञानेश्वर जी ने गीता पर अपनी भावार्थ दीपिका टीका लिखी उस समय उनकी आयु केवल १५ वर्ष की बतायी जाती है । इतनी कम आयु में गीता जैसे गूढग्रन्थ पर सुलझा हुआ भाष्य लिख देना एक चमत्कार ही कहा जायगा ।
तीर्थयात्रा और धर्म प्रचार :
ज्ञानेश्वरी पूरी करने के बाद वे तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थयात्रा का उद्देश्य था लोगों को गीता के माध्यम से अधिक आत्म-कल्याण और ईश्वर प्राप्ति का सरल सुगम मार्गदर्शन दिखाना । कहते हैं कि उनके समकालीन प्रसिद्ध सन्त नामदेव भी इस तीर्थयात्रा में साथ थे । उनके बड़े भाई निवृत्ति नाथ– जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे, सोपानदेव और मुक्ताबाई तो साथ थे ही । साथ में कई और लोग हो गये थे ।
जगह-जगह जाकर उन्होंने सर्व-साधारण को गीता का भावार्थ समझाया । इस ग्रन्थ की भाषा उन्होंने प्रयत्नपूर्वक इतनी सरल रखी कि जन-साधारण को आसानी से वे तथ्य समझ में आ जायें । जहाँजहाँ भी वे जाते भिक्षा-वृत्ति पर निकलते समय गीता सुनने के लिए भी लोगों को निमंत्रित कर देते । पहले दिन जितने लोग उन्हें सुनने आते दूसरे दिन स्रोता बनकर आने वालों की संख्या उससे बढ़ी-चढ़ी ही रहती । क्योंकि ज्ञानेश्वर के वक्तव्यों की भाषा सीधी-सादी होने के साथ-साथ वे कहते समय भावविभोर भी हो उठते । इसके अतिरिक्त वे अविश्वासी और दुराग्रही प्रवृत्ति के लोगों को अध्यात्म की शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए विलक्षण कार्य भी कर बैठते । एक बार कहते हैं उनके प्रतिपादनों की गूढ़ता देखकर कुछ लोगों ने उन पर संदेह किया था कि ये कहीं रटी-रटाई बातें तो नहीं हैं। ज्ञानदेव पर आपेक्ष करते हुए किसी ने कहा था । ‘नाम से क्या होता है ? यह भैंसा जा रहा है । इसको भी ज्ञानदेव कह सकते हैं ।’
इस पर ज्ञानदेव बोले- हाँ-हाँ ठीक है । इसमें और मुझमें कोई भेद नहीं है । इसमें भी मेरी ही आत्मा है।
इतना सुनने पर उस व्यक्ति ने भैंसे की पीठ पर कस कर तीन कोड़े लगाये उस समय ज्ञानेश्वर जी ने सर्वात्मभाव की सिद्धि का अद्भुत परिचय था । कहते हैं कि भैंसे की पीठ पर कोड़े पड़ते ही उसके निशान ज्ञानदेव की पीठ पर उभर आये थे और उन घावों से खून-बहने लगा था । इस प्रकार के बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों और चमत्कारिक दृश्यों ने उपस्थित जनता को ज्ञानेश्वर जी के पक्ष में कर दिया । अब उन्हें पण्डितों की हठधर्मिता की कोई चिन्ता नहीं रही। उससे भी अधिक उन्हें सफलता मिल चुकी थी । वह थी पण्डितों के अनुचित प्रभाव और अवांछनीय धारणाओं में लगाव का तिरोधान ।
कुछ लोग भले ही मान्यताओं के सम्बन्ध में दुराग्रह करते रहें, उससे हानि तो तब है जब जन-साधारण में उनका प्रभाव बना रहे । सन्त ज्ञानेश्वर इस स्थिति को बदलने में बहुत कुछ सफल हो गये थे, इसलिए उन्होंने मूढ़ पण्डितों से उलझना छोड़ दिया । इस घटना के बाद वे कुछ दिनों तक अपने भाई-बहनों सहित पौण ग्राम में ही रहे और धर्म के वास्तविक स्वरूप का लोगों में प्रचार करने लगे।
पौण में लोग उनकी विद्या-बुद्धि और धर्म-दर्शन में प्रवेश से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने विवेक और परमार्थ को ही धर्म का सच्चा स्वरूप निरूपित किया । लोगों के प्रश्न और जिज्ञासाओं का समुचित समाधान करने में उन्होंने अद्भुत कुशलता प्राप्त कर ली । ज्ञानवृद्धि के लिए धर्मशास्त्रों का अध्ययन और मनन-चिन्तन का क्रम भी चलता रहा । फलस्वरूप उनके विद्या भण्डार में वृद्धि होने लगी ।
धर्म प्रचार के लिए उन्होंने उस समय की प्रचलित पद्धति ही अपनाई । कथा-वार्ता और कीर्तन-प्रवचनों के माध्यम से उन्होंने शास्त्रीय सिद्धान्तों को नया सन्दर्भ देना आरम्भ किया । वे प्रतिपादित करते थे कि धर्म और ईश्वर विश्वास ही सब सुखों का केन्द्र तथा कष्ट-कठिनाइयों के निवारण का मार्ग है । दुःख-कष्टों के निवारण में प्रभु विश्वास सहारे का काम देता है । इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के अभाव में धर्म लोगों को अति भावुक और अन्ध श्रद्धालु बना देता है । इस कारण लोग ईश्वर को अपनी कामना पूर्ति तथा अस्वाभाविक लाभों का आधार बना लेते हैं । सन्त ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार की मान्यताओं का खण्डन ही किया और कहा कि ईश्वर की सहायता आत्म बल की वृद्धि, धैर्य-धारण और सद्भावनाओं की प्रेरणा के रूप में ही प्राप्त की जा सकती है।
सच्चिदानन्द-विजय ग्रन्थ की रचना :
पौण से चलकर वे जब नेवा ग्राम में पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने उनका अद्वितीय सन्त और प्रखर ज्ञान सिद्ध महात्मा के रूप में स्वागत किया । अन्ध श्रद्धा और कामना पूर्ति के लिए कई लोगों ने उनसे सहायता की याचना भी की परन्तु ज्ञानेश्वर जी ने पुरुषार्थ और प्रयत्न को ही सफलता का मार्ग बतलाया । नेवा गाँव में एक स्त्री इस कामना से उनके पास आई कि वे उसके मृत पति को जिन्दा कर दें । सन्त ज्ञानेश्वर ने उस स्त्री से पति का नाम पूछा। स्त्री को आशा बंधी कि अब उसका पति जीवित हो जायेगा और उसने नाम बता दिया । मृत व्यक्ति का नाम था- ‘सच्चिदानन्द’ । ज्ञानेश्वर ने तुरन्त कहा- “सच्चिदानन्द तो अमर है । वह कभी मर ही नहीं सकता।”
स्त्री यह सोचकर लौट गई कि उसका पति इतना कहने मात्र से जीवित हो गया होगा। परन्तु घर आकर उसने अपनी आशा के विपरीत पति को उसी अवस्था में पाया । वह फिर ज्ञानेश्वर के पास लौट कर आई । तब उन्होंने जन्म-मरण को प्रकृति का सहज-स्वाभाविक तथा आत्मा की अमरता के सम्बन्ध में विस्तार से समझाया । इन उपदेशों को सुनकर उस स्त्री का शोक सचमुच ही दूर हो गया। उनके वे उपदेश बाद में सच्चिदानन्द-विजय’ नामक ग्रन्थ के रूप में पद्यमय लिपिबद्ध कर लिए गये।
सन्त ज्ञानेश्वर के सम्बन्ध में कई चमत्कारपूर्ण घटनाएँ भी लोक श्रुतियों के रूप में मिलती हैं जिन्हें उन्हें अति मानवी स्वरूप देने के लिए कल्पना रंजित कर दिया गया है अन्यथा उन्होंने धर्म-साधना और ईश्वर-भक्ति की चमत्कारिक सिद्धियों का सदा विरोध ही किया । भगवान् की दी हुई विशेषताओं और योग-साधना के फलस्वरूप अर्जित की गई सिद्धियों और चमत्कारों का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रदर्शन के रूप में करना उनकी दृष्टि में आत्म-कल्याण
में बाधक ही था ।
योगी चांगदेव का शिष्यत्व ग्रहण करना :
चांगदेव नामक एक सिद्ध सन्त उन दिनों ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। वे कई विद्याओं के ज्ञाता तथा परकाया प्रवेश, अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों के स्वामी थे । ताप्ती के तटवर्ती इलाकों में उनकी बड़ी ख्याति थी । सन्त ज्ञानेश्वर ने इन तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश किया तो स्वाभाविक ही उनकी कीर्ति फैली । चांगदेव को उनकी प्रसिद्धि से बड़ी ईर्ष्या हुई । अपना प्रतिस्पर्धी जानकर उन्हें अपमानित करने के लिए चांगदेव ने एक शिष्य को कोरा कागज देकर उनके पास भेजा । ज्ञानेश्वर ने उस कागज को उपस्थित कई लोगों के सामने खोला और चांगदेव के भावों को समझकर उसके जवाब में एक कविता लिखी । जिसमें अद्वितीय ब्रह्मज्ञान और चांगदेव के प्रति सम्मानप्रद भावनाएं व्यक्त की गई थीं।
अपने व्यवहार के प्रत्युत्तर में इतना सद्व्यवहार करते देखकर चांगदेव का हृदय पिघल गया और वे अपने चौदह सौ शिष्यों के साथ सन्त ज्ञानेश्वर के पास आये । सन्त जी उनके आगमन का समाचार सुनकर उनका स्वागत करने के लिए कई मीलों दूर तक स्वयं चल कर आये ।
चांगदेव और भी प्रभावित हुए और बाद में तो उनके शिष्य ही बन गये । सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने इस नये शिष्य को चमत्कारों का प्रदर्शन छोड़कर आत्म-कल्याण की साधना में प्रवृत्त होने का उपदेश दिया ।
सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने सदाशयतापूर्ण व्यवहार और आत्मीयता के प्रभाव से कई लोगों को सही मार्ग पर लगाया । वास्तव में मनुष्य जितना कहता है उससे कहीं अधिक सुना और समझा जाता है क्योंकि उसकी वाणी में उसके हृदय में बसने वाली भावना तथा सम्पर्क में आने वालों के प्रति व्यवहार और सद्गुण ही बल तथा प्रभाव उत्पन्न करते हैं । सन्त ज्ञानेश्वर ने अपने को और मस्तिष्क को ही नहीं व्यवहार और हृदय को भी साधा था। इसी कारण लोग उनके उपदेशों से अधिक उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे।
जलालुद्दीन खिलजी पर संत का प्रभाव :
धर्म प्रचार के लिए वे अपने शिष्यों सहित देश भर की यात्रा पर भी निकले थे। वे घूम-घूम कर ही लोगों को धर्म का उपदेश देते थे । दिल्ली पर उन दिनों कट्टर-पन्थी ‘सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी’ का राज्य था, जो हिन्दू धर्म का कट्टर विरोधी था । उसके शासन में उपासना, पूजा-पाठ, यज्ञ, कीर्तन-भजन आदि सर्वथा निषिद्ध था । सन्त ज्ञानेश्वर को यह सब पता था । फिर भी उन्होंने दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हए भी अपना यह क्रम चालू रखा । भजन-कीर्तन करते हुए वे राजधानी की सड़कों पर घूमने लगे। मौलवियों ने पहले तो मना किया परन्तु जब वे नहीं माने तो उनकी शिकायत सुल्तान से कर दी । सुल्तान ने उन्हें पकड़वाकर बुला लिया । ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी वाणी, अगाध ज्ञान और आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जलालुद्दीन खिलजी ने हिन्दू धर्म पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटा लिए और सब लोगों को अपने धर्म और उपासना की खुली छूट दे दी।
इसी प्रकार सतपुड़ा के एक लुटेरे भील का हृदय परिवर्तन भी उनकी यात्रा के दौरान हुआ था और वह डाकू सन्त ज्ञानेश्वर का निष्ठावान शिष्य बन गया था । सन्त ज्ञानेश्वर ने घूम-घूमकर धर्म का सही मर्म सर्वसाधारण को समझाया तथा उसे स्वयं भी अपने जीवन में उतारा ।
उनकी मान्यता थी कि पूजा-पाठ तब तक अधूरा ही है. जब तक हृदय में सेवा और सद्भावनाएं नहीं जागें । स्वयं गिरी हुई अभावग्रस्त स्थिति से ऊंचे उठे थे । बिना किसी का सहारा लिए स्वयं के प्रयासों से फिर भी गिरे हुए लोगों के प्रति उनके हृदय में पर्याप्त सहानुभूति और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए सहयोग देने की भावना थी। इसके लिए उन्होंने स्वयं भी प्रयत्न किया । चारित्रिक और आत्मिक दृष्टि से गिरे हुओं को ऊँचा उठाया और दीन-दुःखियों के प्रति सेवा. सहयोग की हवा बनाई । श्रद्धाभिव्यक्ति के लिए कई धनवान और सम्पन्न व्यक्ति उन्हें धन-सम्पदा भेंट करने आते रहते थे । अर्पित पैसों की ओर से आँख मूंद कर उसे दीन-दुःखियों की सहायता में लगाने के लिए वे ज्यों का त्यों वापस कर देते।
प्रवचन और उपदेशों द्वारा ही नहीं, लेखनी और क्रियाओं द्वारा भी उन्होंने मानव मूल्यों के प्रतिपादक धर्म का प्रचार किया । भविष्य में भी लोग इन सिद्धान्तों को भूल न जायें, इसका समुचित प्रबन्ध किया । इसी उद्देश्य से उन्होंने साहित्य भी लिखा । उनकी रचित ज्ञानेश्वरी गीता, अमृतानुभव योग वाशिष्ठ-टीका आदि पुस्तकें आज भी आध्यात्मिक साहित्य की अमूल्य सम्पदा मानी जाती हैं । ये सब कृतियाँ उन्होंने अपनी यात्राओं और प्रवासों के समय ही लिखीं ।
आषाढ़ और कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को पंढरपुर में प्राचीनकाल से भारी मेला लगता है । इस अवसर पर देश-देशान्तर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं । उन्हें धर्म के सच्चे स्वरूप से परिचित कराने का सहज-सुलभ अवसर जानकर सन्त ज्ञानेश्वर भी इस मेले में गये । स्थान-स्थान से आये दूर-दूर के लोगों ने उनके सान्निध्य का लाभ उठाया । इस मेले में कुछ विरोधियों ने उनसे पूछा कि “आप महान् सन्त और ज्ञानी हैं तो घर बैठकर ही क्यों नहीं पुजते ? इधर-उधर भटकते रहने की क्या जरूरत है ?”
ज्ञानेश्वर जी ने कहा- “जगह-जगह घूमकर लोगों को ज्ञान और सन्मार्ग दिखाना तो मेरा धर्म है । कुँआ प्यासे के पास नहीं जाता, इसलिए वह छोटा ही रह जाता है । सूखे तथा जरूरत के क्षेत्रों में नदी बहती है तो वह अणु से विभु, क्षुद्र से महान् और छोटी जलधारा से सागर बन जाती है । यह समझकर ही मैं भी अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यत्र-तत्र भटकता रहता हूँ।” कितना सटीक उत्तर था उनका । सन्त महापुरुषों की लोक हित साधना भी उनके आत्म-कल्याण में सहायक बन जाती है ।
कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर जी ने एक बार गधे के मुँह से भी वेद ऋचाओं का पाठ करवाया था । तीर्थ यात्रा द्वारा गाँव-गाँव में भक्तिमार्ग का प्रचार कर ज्ञानेश्वर जी वापस पंढरपुर लौटे । उन्होंने आत्म-कल्याण के लिए जिस मार्ग का उपदेश दिया उसमें ज्ञानकर्म और भक्ति का अद्भुत समन्वय है । अपने-अपने मत की पुष्टि के लिए अधिकांश आचार्यों ने किसी एक पर ही अधिक जोर दिया है। जैसे शंकराचार्य ने ज्ञान को ही सर्वाधिक प्रधानता दी है तथा कर्म और भक्ति को गौण बताया है लेकिन ज्ञानेश्वर ने ज्ञान, भक्ति और योग तीनों विषयों का समुचित विश्लेषण करते हुए साधक से अपनी रुचि के अनुकूल मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी है।
संत की महासमाधि :
ज्ञानेश्वर जी ने अपनी ज्ञानधारा प्रयाग से लेकर वृन्दावन, पंजाब, मारवाड़, काशी, गिरनार आदि स्थानों पर बहाई और मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों तथा स्थानों को उस ज्ञान गंगा में स्नान कराते गये। तीर्थ यात्रा पूरी कर लेने के बाद पंढरपुर में ही उन्होंने सन् १२९६ में समाधि ले ली । ज्ञानेश्वरी गीता के अतिरिक्त योगवाशिष्ठ पर भी उन्होंने अमृतानुभव नाम की एक टीका लिखी है । उनके उपदेशों से समाज में पिछड़े और निम्नकुल के लोगों में आत्मविश्वास का भाव जागा । बड़े-बड़े शास्त्रियों और धर्मगुरुओं ने उन्हें जब सर्व धर्म के लाभ से ही वंचित कर रखा था तब ज्ञानेश्वर जी ने उनके लिए ईश्वरीय राज्य का द्वार खोला और धार्मिक क्षेत्र में समानता का आदर्श स्थापित किया।
आगे पढ़ने के लिए कुछ अन्य सुझाव :
• श्री रमण महर्षि का जीवन परिचय
• प्रेरक प्रसंग – सम्राट अशोक का महान पुत्र महेन्द्र
• स्वामी रामतीर्थ जी का जीवन परिचय